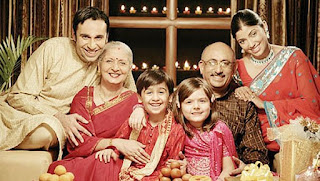प्राचीन समय में ,इतना पुराना भी नहीं कह सकते ,लगता है ,जैसे कल ही की बात हो ,परिवार कितने बड़े होते थे ?उन्हें देखकर ही 'संयुक्त परिवार 'नाम पड़ा। उस संयुक्त परिवार में दादा -दादी ,चाचा -चाची ,ताऊ और ताई जैसे रिश्ते होते ,उनके बच्चे ,इस तरह कम से कम बीस -पच्चीस लोगों का परिवार होता था। परिवार में एक -दूसरे के साथ मिल -जुलकर एक साथ तीज -त्यौहार मनाते ख़ुशियाँ बांटते ,सब प्रसन्न रहते थे। कम सुविधाओं में भी प्रसन्न रहते। जो पढ़ते ,वो बाहर नौकरी पर चले जाते और जो नहीं पढ़ पाते वो खेती संभाल लेते इस तरह संतुलन बना रहता। परिवार के वृद्धजन उस परिवार का संरक्षण कर ,उन्हें एकजुट रखने का प्रयत्न करते अपनी नई पीढ़ी को उनके पूर्वजों से अवगत कराते। खेल ही खेल में या बातों ही बातों में बच्चों को बहुत कुछ सिखा जाते ,जैसे पहेली पूछकर अथवा कोई भी कटवा पहाड़ा पूछते
,रामायण -महाभारत में से कोई भी किस्सा सुना देते या फिर कोई संक्षिप्त प्रश्न पूछ डालते जिससे बच्चा उन्हें बताने के लिए दिमाग पर ज़ोर लगाता। आज हर चीज़ बच्चे को पढ़नी पड़ती है ,अथवा रटनी भी पड़ती है और दबाव में जो रटता है उस समय तो याद हो भी जाये किन्तु कुछ समय पश्चात भूल जाता है। पढ़ाई का दबाव इस कदर रहता है कि पुस्तकें देखते ही उनसे दूर भागता है या बचने का प्रयत्न करता है।
,रामायण -महाभारत में से कोई भी किस्सा सुना देते या फिर कोई संक्षिप्त प्रश्न पूछ डालते जिससे बच्चा उन्हें बताने के लिए दिमाग पर ज़ोर लगाता। आज हर चीज़ बच्चे को पढ़नी पड़ती है ,अथवा रटनी भी पड़ती है और दबाव में जो रटता है उस समय तो याद हो भी जाये किन्तु कुछ समय पश्चात भूल जाता है। पढ़ाई का दबाव इस कदर रहता है कि पुस्तकें देखते ही उनसे दूर भागता है या बचने का प्रयत्न करता है।
आजकल तो अँग्रेजी स्कूलों का बोलबाला है ,बच्चा ठीक से बोलना भी नहीं सीख़ पाता और उसका बचपन अपने दादा -दादी के साथ नहीं ''प्ले स्कूलों ''में बीतता है ,वहां माता -पिता से दूर बच्चा रोता है ,क्योंकि माता -पिता के पास समय नहीं। वहां सीखता है ,2 *1 =2 सीखता है ,जो कुछ समय बाद भूल भी जाता है। ख़ैर छोड़िये !यहां बात शिक्षा की नहीं ,परिवार की हो रही है। अब देखिये, शैतान ने अपना खेल खेला, उसे इस तरह एकजुट लोग पसंद नहीं आये। जो बच्चे ख़ुशी -ख़ुशी अपने खेतों में काम करते थे ,उन्हें लगने लगा -हम यहाँ मिटटी में खेती -बाड़ी करते हैं और ये लोग शहर में गुलछर्रे उड़ाते हैं। ये साहब बनकर आते हैं और हम गाँव के' गवाँर 'कहलाते है। ऐसी मानसिकता के कारण परिवारों का' विघटन 'होना आरम्भ हो गया। एक बड़े परिवार के टुकड़े होकर चार परिवारों में परिवर्तित हो गए। खेती से मुख मोड़ने लगे और अपने -अपने बच्चों को पढ़ाकर ,सभी साहब बनाने के लिए शहर की ओर रुख़ करने लगे। जिसके परिणामस्वरूप हमारे क्षेत्र [खेत ]घटने लगे। जमीनें या तो बिकने लगीं या ठेकों पर दी जातीं । जिन जमीनों पर उनके पूर्वजों ने खून -पसीना एक किया ,अब वे जमीनें बंटकर 'कौड़ियों 'के दाम जाने लगीं। कई -कई एकड़ ,बीघों के मालिक ,शहरों में जाकर नौकर बन गए। ज्यादा पढ़ा -लिखा तो बड़ा नौकर ,कम पढ़ा -लिखा उससे छोटा नौकर ,क्योंकि लोगों को उसमें ही भविष्य नज़र आने लगा। उन्हें अपनी मातृभूमि ,जन्मभूमि से कोई लगाव ही नहीं रहा।
आधुनिकता की दौड़ में ,सब दौड़ लगाने लगे ,कई बार तो दौड़ लगाते -लगाते थक भी जाते तो जायें कहाँ ?वापस लौटने का दरवाज़ा तो वो स्वयं ही बंद कर आये। अब यही कर्मभूमि है ,सोचकर जीवन भर संघर्ष करने में ही, इसे अपनी नियति मान लिया। इससे परिवार और' विघटित' होते चले गए। भाई तो अलग हुए किन्तु माता -पिता या तो अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर रहते या फिर बच्चों में बंट जाते। अब परिवारों में दादा -दादी ,माता -पिता और बच्चे रह गए। बच्चे भी घटकर चार -पांच से घटकर दो रह गए , क्योंकि बढ़ती महंगाई और बढ़ती आबादी से भी तो जूझना है और देश के अच्छे नागरिक होने के नाते हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि परिवार में ''दो ही बच्चे ,सबसे अच्छे ''समय भी परिवर्तनशील है। परिवर्तन के साथ -साथ इन दो बच्चों पर मानसिक दबाब अधिक पड़ गया ,जिसके परिणामस्वरूप उन्हें छुटपन में ही पाठशाला में डाला जाता और फिर उन पर अपनी आशाएं ,अपेक्षाएं थोपी जाती। चाहे उसका मष्तिष्क उसके लिए अभी परिपक़्व हुआ हो या नहीं। पहले बच्चों पर किसी भी तरह का दबाब नहीं था कि पढ़ना ही है ,बहुत सी चीज़ें तो वो घर में ही सीख़ जाता था। उस पर किसी भी तरह का दबाब नहीं होता था। नहीं पढ़ना तो खेती कर लो ,माता -पिता भी खुश ,बच्चा भी। आठ -दस बच्चे अभावों में भी पल जाते थे। आज एक ही बच्चा सारी अपेक्षाएं और उपेक्षाएँ सब झेलता है। आजकल तो एक बच्चा पालना ही ऐसा है जैसे हाथी पाल लिया हो।
बच्चों पर इतना दबाब पढ़ाई का ,उससे निकलकर रोजगार के लिए सोचने में ही इतना समय व्यतीत हो जाता है कि वो परिवार बसाने की तो सोच ही नहीं सकता। देर से शादी और देर से ही बच्चे होते हैं क्योंकि सुविधाओं को जुटाने में इतना व्यस्त हो जाता है ,परिवार आगे बढ़ाने के लिए भी बहुत सोचना -समझना पड़ता है , और कई बार तो इतनी देर हो चुकी होती है ,परिवार की एक पीढ़ी तो जा चुकी होती है। दादा -दादी बच भी जायें तो वो इतने बूढ़े और बिमार हो जाते हैं कि बच्चों को कहानी -किस्से क्या सुनाएंगे वो अपनी परेशनियों से ही नहीं निकल पाते हैं। और परिवार में सास -ससुर और एक बेटा -बहु रह जाते हैं। आज के समय में हमारे परिवारों में तीन या चार लोग रह जाते हैं ,जिन्हें बच्चे अपनी पुस्तक में पढ़ते हैं ,'एकल परिवार '.इन परिवारों में भी बहु अच्छी हो, तो समय से रोटी नसीब हो जाती है। आजकल की हमारी भारतीय नारी अब वो अबला या बेचारी नहीं रही ,आज वो अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसके साथ कमाने निकल जाती है ,क्योंकि इच्छाएं अनंत हैं। परिणामतः सास दिनभर करे भी क्या ?कम से कम एक नौकर का खर्चा तो बचा ही सकती है ,वरना अपने पति के बनाये घर में एकांतवास करती है। यदि बहु नौकरी भी नहीं करती है तो किट्टी में जाने के लिए समय है किन्तु घर में बुजुर्ग के लिए दो रोटी बनाने का समय नहीं। रिश्तों का कोई लिहाज़ नहीं ,न ही उम्र का। ''मैं क्या तुम्हारे घर में नौकर बनकर आयी हूँ ''ये वाक्य आजकल अधिकतर घरों में सुनने को मिल सकते हैं। परिवार विघटित होकर पति -पत्नी और बच्चा तक सीमित रह गए। घर आधुनिक साधनों से पूर्ण होंगे ,हर तरह की सुविधाएँ होंगी किन्तु उस घर में किसी भी बुजुर्ग़ के लिए स्थान नहीं होगा।जिस तरह ''कबूतर खाने ''जैसे दो कमरों के फ्लैट छोटे हो गए , ऐसे ही लोगों के दिल हो गए। उन लाखों -करोड़ों के मकानों में वो स्वार्थी लोग प्रसन्न रहते हैं ,अपना पतन होते देख खुश होते हैं। इन छोटे मकानों अथवा परिवारों में न ही किसी तरह के संस्कार, न ही रीति -रिवाज़ दिखते हैं। ज़मीन से भी इतनी दूरी ,आसमान को छूते नज़र आते हैं ,तो अपने देश की मिटटी अथवा जन्मभूमि से किस तरह प्रेम होगा ? जिसकी गोद में खेले ही नहीं और जिसका दूध पीया उसका तो सम्मान समाप्तप्रायः ही है।
कंकड़ -पत्थर में पलकर ,ऐसे ही दिल भी हो गए ,संस्कार किस चिड़िया का नाम है ?शायद ही जानते हों। आजकल की पत्नियां ,अपने पति को उसके परिवार से ही दूर कर देती हैं ,उनसे कैसी उम्मीद की जा सकती है ?उनके लिए तो उनका मायका ही परिवार है। पति चाहते हुए भी अपने परिवार से मिल नहीं पाता ,कोई -कोई विरोध भी करता है तो वही पारिवारिक क्लेश झेलता है। बहुत से इन परिस्थितियों से समझौता कर भी लेते हैं ,बहुतों के लिए तो विवाह होते ही, रिश्ते बेगाने हो जाते हैं। अभी मुझे एक किस्सा याद आया -एक महाशय ,अपनी बेटी के लिए लड़का ढूँढ रहे थे और उनकी शर्त ये थी कि मेरी बेटी तो कमाती है ,वो तो खाना नहीं बनाएगी ,अब जैसे भी उन्हें लड़का मिला किन्तु अभी कुछ दिनों पहले मुलाकात हुई तो बेटे के लिए वधु की तलाश में थे ,सुंदर ,सुशील ,पढ़ी -लिखी बहु चाहिए थी। जब मैंने पूछा -बहु से खाना तो नहीं बनवाएंगें ,तो बोले -कौनसा उसे ,कुनबे का खाना बनाना है ,परिवार में हम तीन ही लोग तो हैं। मैंने पूछा -अब परिवार रहे ही कहाँ ?ये ही सोच बेटी के लिए क्यों नहीं थी ?ऐसी ''दोगली ''सोच के कारण ही घरों का विघटन होता जा रहा है। और रिश्तों की तो छोड़ो, पति को ही समय पर खाना मिल जाये यही बहुत है ,इस पर भी झगड़े होते हैं।
अब तो आने वाली पीढ़ी का विवाह से ही विश्वास उठता जा रहा है।
सब सुविधाएँ चाहिए किन्तु परिवार के साथ सामंजस्य बैठाना नहीं चाहते।
व्यक्ति आरामपसंद ज्यादा हो गया है। रिश्तों से ज्यादा पैसे और सुविधाओं से ज्यादा लगाव भी परिवार के विघटन का कारण है।
अब बड़ों की इज्ज़त और लज्ज़ा तो रही ही नहीं।
भौतिकवादी वस्तुओं का आदि होता जा रहा है।
अब तो रिश्तों में भावनात्मक लगाव भी नहीं रहा।